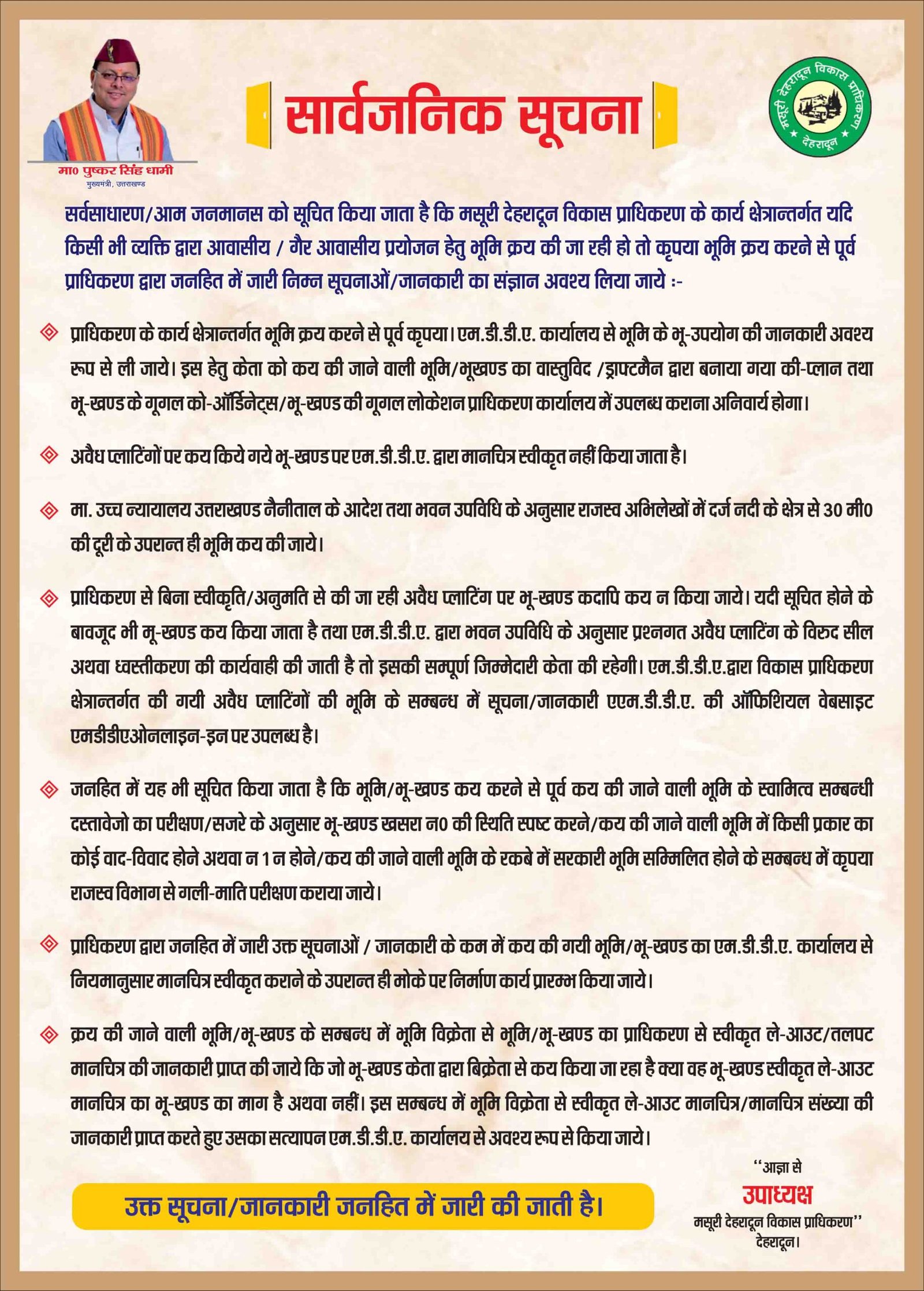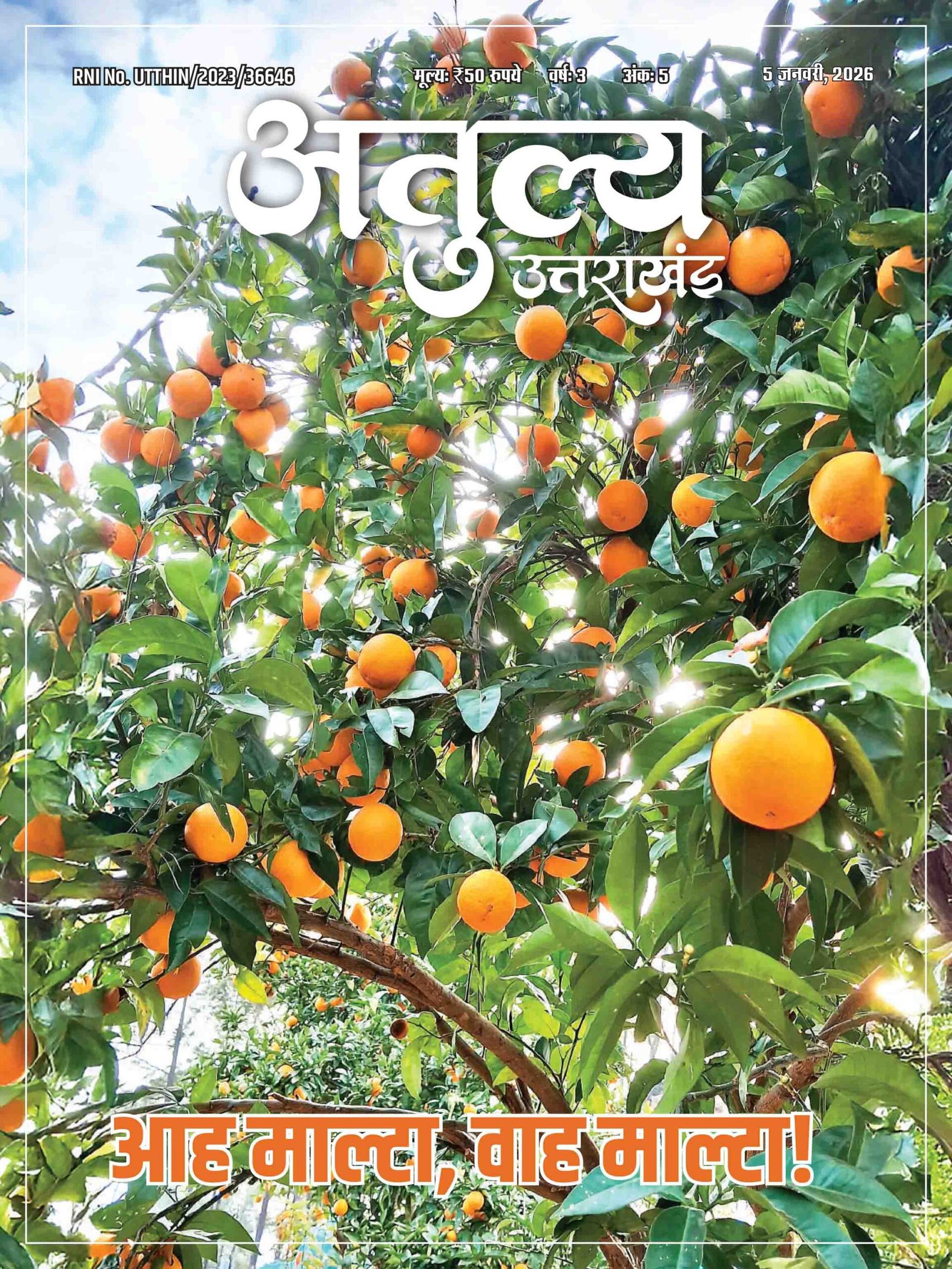Ground Reality : नीति-नियंताओं की ये प्राथमिकता रही है कि वह चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हरसंभव सुविधा दे सकें। कोशिश की जाती रही हैं कि इस यात्रा को सुगम बनाया जाए, हो भी क्यों ना। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यह यात्रा सदियों से पहाड़ की आजीविका का मुख्य स्रोत रही है। एक तरफ नीति-निर्माता हैं, जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन के लिए पहुंचें वहीं, दूसरी तरफ वो पर्यावरणविद हैं जो ऐसा नहीं चाहते। इकोनॉमी (अर्थव्यवस्था) और इकोलॉजी (पारिस्थितिकी) के बीच की ये लड़ाई उत्तराखंड के इतिहास में भरी पड़ी है। चार धाम यात्रा के संदर्भ में इस लड़ाई का मुख्य अखाड़ा बनी है एक परियोजना। नाम है- चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। इस पर पर्यावरणविद लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसे हिमालय के लिए खतरा बता रहे हैं। दूसरी तरफ, सरकार इस परियोजना को अनिवार्य बताती है। अनिवार्य सुगम चार धाम यात्रा और भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा के लिए। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि भला ऐसी परियोजना जिससे चार धाम यात्रा आसान होगी, जिससे सीमा ज्यादा सुरक्षित होगी, उसका कई लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों इस परियोजना को रोकने के लिए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी? इन सभी सवालों का जवाब खोजने की कोशिश है ये रिपोर्ट…।
27 दिसंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार धाम महामार्ग विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इस 889 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 2 लेन की हाइवे बनाने की योजना थी, जिसमें हाइवे को पहले 12 बाद में 10 मीटर चौड़ा करने का प्लान शामिल है। इस योजना के तहत चार धाम रूट पर 16 बाइपास रोड, 15 बड़े फ्लाइओवर, 101 छोटे ब्रिज, 3500 से ज्यादा कलवर्ट और 2 टनल बनाई जा रही हैं। 2023 में जिस सिलक्यारा टनल में मजदूर फंसे थे, वह भी इसी का हिस्सा है। चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत सारा काम प्रमुख तौर पर ऋषिकेश-माणा, ऋषिकेश-गंगोत्री और टनकपुर-पिथौरागढ़ के बीच गुजरने वाली नेशनल हाइवे 58, 94, 108, 109 और नेशनल हाइवे 125 पर हो रहा है। इस पूरे काम को करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार 12 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं। जब इस परियोजना की शुरुआत हुई तब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि भूस्खलन से बचने, सुरक्षा के लिए पुराने भूस्खलन और धंसने वाले स्थानों का स्थिरीकरण किया जा रहा है। कमजोर भूमि पर वनस्पति विकास के लिए हाइड्रो सीडिंग जैसी जैव इंजीनियरिंग विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

कहा गया कि ये तकनीक राजमार्ग और बस्तियों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रखेंगी। लेकिन जितने बड़े दावे किए गए, उतना जमीन पर हुआ कि नहीं, ये आप आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि इस योजना पर 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। इसमें उत्तराखंड राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) शामिल है। जुलाई, 2023 में केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि 601 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इस योजना को वैसे तो 2020 तक पूरा हो जाना था लेकिन अलग-अलग कोर्ट में पर्यावरण मंजूरी संबंधित मुकदमेबाजी की वजह से इसमें देरी हुई।
चार धाम रोड प्रोजेक्ट क्यों?
इस योजना के पक्ष में सरकार ने दो फायदे गिनाए थे। पहला, उत्तराखंड में चारों धाम तक सफर आसान होगा। इससे उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। दूसरा, ये परियोजना देश की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड की सीमा नेपाल और चीन से लगती है। ऐसे में सीमा तक पहुंचने वाली सड़कें चौड़ी होंगी तो यहां महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों को पहुंचाना आसान होगा। सरकार की तरफ से दिए गए तर्क सब सही नजर आ रहे थे लेकिन 2018 में इस प्रोजेक्ट को लेकर तब बहस तेज हो गई जब एक NGO इस परियोजना के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गया।
कोर्ट में चार धाम रोड प्रोजेक्ट
चार धाम रोड परियोजना की जिस दिन से घोषणा हुई, उस दिन से ही इसके विरोध में सुर उठने लगे थे लेकिन 2018 में ये मामला कोर्ट जा पहुंचा। इस परियोजना के खिलाफ 27 फरवरी, 2018 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दाखिल की गई। सिटीजंस फॉर ग्रीन दून एनजीओ ने अपनी याचिका में आरोप लगाए कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसका हिमालय पर बुरा असर पड़ रहा है। कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों का कटान हो रहा है। ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग की जा रही है। एनजीटी में दर्ज याचिका में ये भी बताया गया कि निर्माण कार्य में पैदा हो रहे कचरे को भागीरथी नदी में डंप किया जा रहा है। एनजीओ ने यहां भूस्खलन बढ़ने और मिट्टी का कटाव बेतहाशा होने पर चिंता जताई। एनजीओ ने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट का इनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट यानी प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इसका आकलन भी नहीं किया। इसके जवाब में सरकार ने ट्रिब्यूनल को बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना बनता ही नहीं है।
सरकार ने कोर्ट में जानकारी दी कि इस परियोजना को 53 छोटे-छोटे स्ट्रेच में बांटा है। हर स्ट्रेच की लंबाई 100 किलोमीटर और चौड़ाई 40 मीटर से कम है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़े साल 2013 के संशोधन का हवाला दिया। केंद्र ने बताया कि इस संशोधन के मुताबिक मौजूदा हाइवे में अगर 100 किलोमीटर से कम की लंबाई है तो इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं है। इन दलीलों के आधार पर 26 सितंबर, 2018 को एनजीटी ने अपना फैसला सुनाया। एनजीटी ने अपने फैसले में कहा, ‘क्योंकि ये प्रोजेक्ट छोटे-छोटे स्ट्रेच में बंटा हुआ है और ये स्ट्रेच 100 किलोमीटर से कम के हैं तो प्रोजेक्ट को ईआईए यानी इनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट की जरूरत नहीं है।‘ भले ही एनजीटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था लेकिन पर्यावरण को लेकर वह चिंतित जरूर दिखा। यही वजह है कि एनजीटी ने एक ओवरसाइट कमिटी बनाने का निर्देश भी दिया। इस कमिटी की जिम्मेदारी ये होती कि प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान पर्यावरण के हितों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, इस पर नजर रखे। हालांकि एनजीटी का फैसला लागू हो पाता, उससे पहले इस फैसले को सिटीजंस फॉर ग्रीन दून ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 8 अगस्त, 2019 को ओवरसाइट कमिटी की जगह हाई पावर कमिटी (एचपीसी) बनाने के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणविद् प्रोफेसर रवि चोपड़ा को इस कमिटी का अध्यक्ष बनाया। कोर्ट ने इस कमिटी को पूरे चार धाम रोड प्रोजेक्ट की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी। एचपीसी को काम सौंपा गया कि वह चार धाम रोड प्रोजेक्ट की हर पहलू से जांच करे और इसका पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का आकलन कर 4 महीने में रिपोर्ट सौंपे। एचपीसी ने 13 जुलाई, 2020 को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। एचपीसी वैसे तो लगभग सभी मुद्दों पर एकमत थी लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर कमिटी में दो मत हो चले थे। एचपीसी के 13 सदस्य, जिसमें ज्यादातर सरकारी अधिकारी शामिल थे, वह हाइवे की चौड़ाई को 12 मीटर रखना चाहते थे। वहीं, कमिटी के अध्यक्ष समेत 5 मेंबर्स चौड़ाई को 5.5 मीटर तक सीमित रखना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों के सुझाव को स्वीकारा और सरकार को सड़कों को 5.5 मीटर तक चौड़ी करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य पहले की व्यवस्था के आधार पर चलता रहा। एचपीसी अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने कई पत्र सुप्रीम कोर्ट को लिखे जिनमें बताया गया कि किस तरह कोर्ट के आदेश के बावजूद सड़कों का निर्माण पुराने मानकों के आधार पर ही हो रहा है। उन्होंने बताया कि एनएच-58 और एनएच-94 पर पहले की तरह ही पहाड़ों और पेड़ों को काटा जा रहा है। इस बीच, स्वामी संविदानंद ने भी एक एफिडेविट सब्मिट किया। इसमें भी अपील की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पहाड़ों के कटान और पेड़ों को गिराने के काम पर रोक लगाई जाए।

दूसरी तरफ से सरकार भी एक्टिव हो गई और अब रक्षा मंत्रालय भी पिक्चर में आ गया। रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। रक्षा मंत्रालय ने अपनी याचिका में कहा कि सैन्य जरूरतों के लिए जरूरी है कि कैरिज-वे की चौड़ाई 7 मीटर और पेव्ड सोल्डर 1.5 मीटर चौड़ा हो। कैरिज-वे का मतलब मुख्य सड़क के उस हिस्से से है जहां पर वाहन केवल एक दिशा में जाते हैं। रक्षा मंत्रालय का तर्क था कि भारत-चीन सीमा तक जरूरी संसाधन पहुंचाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण जरूरी है। इस पर 2 दिसंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमिटी को निर्देश दिए कि वह रवि चोपड़ा की तरफ से की गई शिकायतों के साथ ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से उठाई गई बात पर चर्चा करे और रिपोर्ट सौंपे। रिपोर्ट सौंपी गई और कहा गया कि सेना को आए दिन भूस्खलन से जूझने वाली सड़कें देने से अच्छा है कि उन्हें वो सड़कें दी जाएं जो लंबे समय तक सस्टेन करेंगी। यानि कि 5.5 मीटर चौड़ीकरण का ही फिर समर्थन किया गया। हालांकि केंद्र सरकार का सैन्य जरूरत वाला एंगल सुप्रीम कोर्ट में जीत गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2021 में सैन्य जरूरतों को देखते हुए चार धाम रोड़ प्रोजेक्ट में सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी और साथ में ही एक ओवरसाइट कमिटी भी बनाई जो पर्यावरणीय चिंताओं का ध्यान रखेगी। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि कमिटी नए सिरे से एनवायरनमेंट एसेसमेंट नहीं करेगी। इस तरह चार धाम रोड प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रहा।
चार धाम रोड प्रोजेक्ट का विरोध क्यों?
चार धाम रोड प्रोजेक्ट का विरोध क्यों? इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है और वो है कि सड़कों का जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, वो ऐसे किया जा रहा है जिससे इस पूरे हिमालयी क्षेत्र को फायदा कम, नुकसान ज्यादा पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमिटी के सदस्य रहे हेमंत ध्यानी इस बात को सरल शब्दों में समझाते हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर काम करने वाले ‘इंडिया स्पेंड’ से बात करते हुए ध्यानी बताते हैं कि पहाड़ में सड़कों को जितना अधिक चौड़ा किया जाएगा, उतना ही पहाड़ों को काटना होगा। जितने पहाड़ कटेंगे उतना ही नुकसान प्रकृति को होगा। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पेड़ों के साथ पहाड़ों को काटना होगा और इससे निकलने वाले मलबे का निस्तारण करना पड़ेगा। यही चीजें हैं, जो खतरनाक साबित हो रही हैं। ‘इंडिया स्पेंड’ की ही रिपोर्ट बताती है कि 2021 तक इस परियोजना के लिए 60 हजार पेड़ काटे गए हैं। जो पेड़ काटे गए, उनके तनों की मोटाई 30 सेंटीमीटर से अधिक थी। बड़े पेड़ पहाड़ को बांधे रखते हैं। इससे मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। लेकिन जब ऐसे पेड़ ही काट दिए जाएंगे तो मिट्टी का कटाव बढ़ेगा और कमजोर पहाड़ भूस्खलन के तौर पर नीचे आएंगे और तबाही मचाएंगे। ‘इंडिया स्पेंड’ की रिपोर्ट बताती है कि चार धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत कई जगहों पर 90 डिग्री पर स्लोप काटे जा रहे हैं। इससे नए भूस्खलन क्षेत्र तैयार हो गए हैं।
इसके अलावा 2023 की एशिया पैसिफिक नेटवर्क ऑफ इनवायरमेंट डिफेंडर्स की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी निर्देशों के बावजूद कई ठेकेदार स्लोप काटने के बाद उन्हें ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इससे भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। पहाड़ों की कटाई से निकलने वाला मलबा भी एक बड़ा मुद्दा है। सरकार ने भले ही इसके निस्तारण के लिए कई डंपिंग जोन बनाए हैं लेकिन एशिया पैसिफिक नेटवर्क की रिपोर्ट बताती है कि मलबे को डंपिंग जोन में डालने की बजाय स्लोप पर ही छोड़ दिया जा रहा है। इसकी एक वजह डंपिंग जोन का फुल होना भी संभव है। 2021 में ही कई रिपोर्ट्स आईं थीं जिनमें बताया गया था कि डंपिंग जोन में क्षमता से ज्यादा मलबा डंप किया जा रहा है। क्षमता से ज्यादा मलबा डालने का मतलब है कि भूस्खलन को न्यौता देना। सिर्फ यही नहीं, डंपिंग जोन में डाले गए मलबे से क्षेत्र में पैदा होने वाले बांज, बुरांस जैसे अमूल्य पेड़ों के साथ-साथ खेत और नदी के प्रवाह को भी नुकसान पहुंचता है लेकिन इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि हिमालय अभी नए पहाड़ हैं। ऐसे में यहां सड़कों को बनाने के लिए किए जा रहे ब्लास्ट इन्हें और खोखला कर रहे हैं। इसकी वजह से भूस्खलन के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। लगता है जैसे कि इस बात का कुछ हद तक अहसास सरकार को भी हो गया है। हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि वह भागिरथी इकोनॉमिक जोन की रक्षा के लिए पेड़ नहीं काटेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे प्रोजेक्ट की लागत और बढ़ जाए लेकिन पेड़ ना काटने पड़े, इसको लेकर कुछ समाधान किया जाएगा। हालांकि ये वादे जमीन पर कितने हकीकत का रूप लेते हैं, इसका अभी इंतजार है। क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट्स खुद सरकार ने पेश की थीं जो हिमालय में सड़कों के चौड़ीकरण पर सवाल उठा रही थीं।

चार धाम रोड प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए कैसे सरकार ने अपनी ही तय की हुई नीतियों को दरकिनार किया, उसके कई उदाहरण मिलते हैं। सबसे बड़ा आरोप जो पर्यावरणविद सरकार पर लगाते हैं, वो ये कि सरकार ने जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को 53 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट में बांटा। जानबूझकर इन छोटे-छोटे स्ट्रेच को 100 किलोमीटर के अंदर रखा गया। इस तरह सरकार के लिए इनवायरमेंट एसेसमेंट से बचना आसान हो गया। एक आरोप ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रोजेक्ट के तहत सड़क को 5.5 मीटर तक चौड़ी करने पर मुहर लगा दी तो खुद रक्षा मंत्रालय इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस तरह सैन्य जरूरत का एंगल लाया गया। खुद रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि सेना प्रमुख ने मौजूदा रोड यानी कि चार धाम रोड प्रोजेक्ट से पहले की रोड को सैन्य जरूरतों के लिए काफी कहा था। हालांकि इस याचिका को डालते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अब सेना की जरूरतें बढ़ गई हैं और इसलिए उसे चौड़ी सड़कें चाहिए। सिर्फ यही नहीं, आज भले ही केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्रालय लगातार चार धाम रोड प्रोजेक्ट को सारी चिंताओं को नजरअंदाज कर पूरा करने में जुटा हुआ हो लेकिन 2018 में मंत्रालय के विचार इसके उलट थे। 2018 में खुद परिवहन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया। मार्च, 2018 के इस सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई इंटमिडियएट विड्थ यानी कि 5.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
हाई पावर कमेटी के एक धड़े ने भी इस सर्कुलर का हवाला दिया था लेकिन चार धाम रोड प्रोजेक्ट के मामले में इसे खुद सरकार ने नकार दिया। केंद्र सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक मिशन डॉक्युमेंट 2010 बनाया था। इसमें भी यही कहा गया था कि सड़कों के निर्माण के दौरान संबंधित क्षेत्र के भूगोल की संवेदनशीलता को ही ध्यान में रखकर निर्माण किया जाना चाहिए। इस डॉक्युमेंट में ये भी कहा गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर से ज्यादा की राष्ट्रीय सड़कें हों या नेशनल हाइवे, इनके लिए इनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अनिवार्य होना चाहिए। फिर चाहे इसमें सड़कों का चौड़ीकरण भी क्यों ना शामिल हो। इसी डॉक्युमेंट में ये भी कहा गया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण के दौरान जो भी खराबी तैयार होती है, उसे ठीक किया जाना चाहिए लेकिन पर्यावरणविदों की मानें तो ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। एक तर्क इस परियोजना के सपोर्ट में ये दिया गया था कि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन खुद केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग को ऐसा नहीं लगता। नीति आयोग ने 2018 की अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि हिमालयी क्षेत्र में जो मौजूदा टूरिज्म का स्वरूप है, वो कतई सस्टेनेबल नहीं है। नीति आयोग ने आगे कहा कि टूरिज्म का ये स्वरूप परंपरागत आर्किटेक्चर को नए खतरनाक निर्माण से बदल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह यहां पर खराब तरीके से सड़कों का निर्माण किया जाता है।

2013 केदारनाथ आपदा पर केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन पर नजर रखने वाली बॉडी ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पहाड़ी इलाकों में सड़कों का निर्माण ही यहां के इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसकी वजह से यहां के ड्रेनेज पैटर्न में काफी बड़े बदलाव आते हैं और मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है। इससे पेड़ कटान समेत दूसरी दिक्कतें भी पेश आती हैं। एक्सपर्ट्स और पर्यावरणविद इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर अब तक, सिर्फ यही कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण जिस तरह से हो रहा है, वो कतई भी हिमालय के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। और इन चेतावनियों को सच होते हुए हम आए दिन देख रहे हैं। लगातार चार धाम रूट पर भूस्खलन और रोड ब्लॉक होने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।
ऐसा नहीं है कि पहाड़ के रहने वाले लोग या फिर पर्यावरणविद पहाड़ों में विकास कार्य के खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरह से ये विकास कार्य किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सब आवाज उठा रहे हैं। चार धाम रोड परियोजना का विरोध नहीं है लेकिन इस परियोजना के नाम पर जिस तरह पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं।