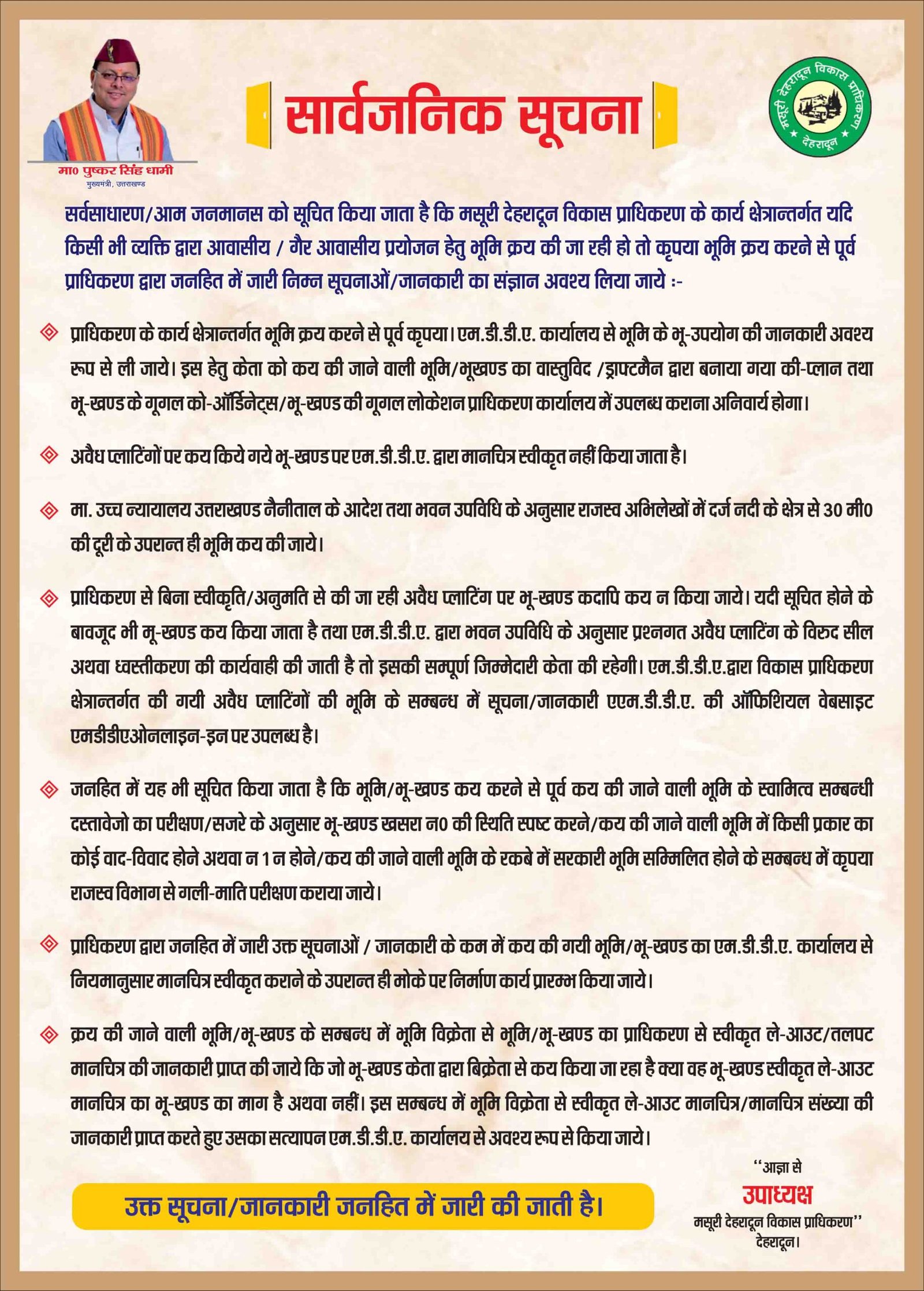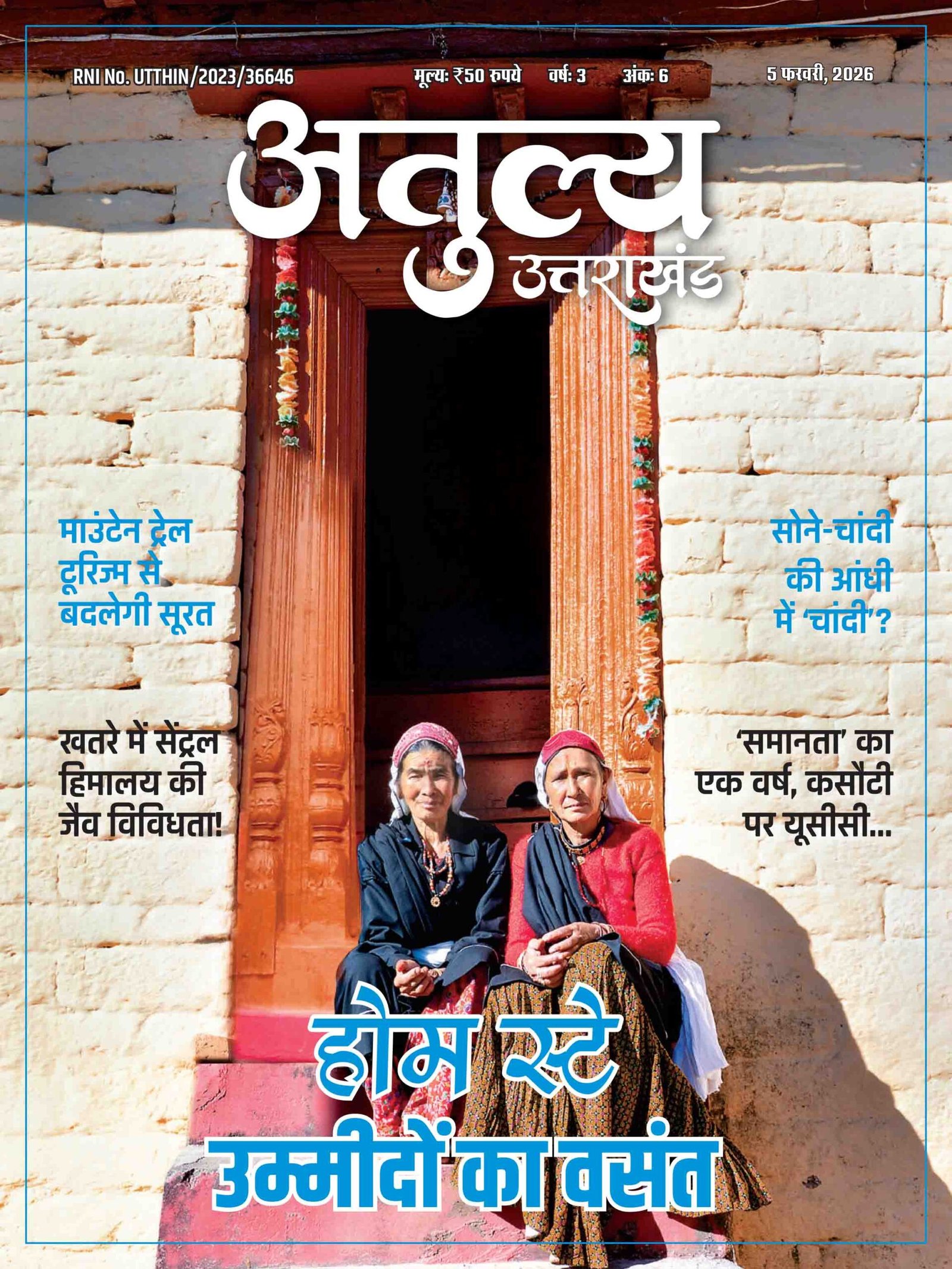- महेश चंद्र पुनेठा –

हमारी शिक्षा व्यवस्था कई संकटों से घिरी हुई है। कुछ नीतिगत, व्यवस्थागत और कुछ क्रियान्वयन के स्तर पर हीलहवाली के कारण। इन संकटों पर समय-समय पर बहुत सारी बातें औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होती रही हैं। इसलिए उनकी पुनः चर्चा न कर उन संकटों के समाधान पर अपनी बात रखते हुए सभी के साथ एक अनुभव बांटना चाहूंगा। मेरा मानना है कि मौजूदा शिक्षा के संकटों के समाधान के लिए हमें दो मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। पहला , वह नीतियां जो सार्वजनिक शिक्षा को कमजोर करने तथा उसके व्यवसायीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ना। दूसरा, सरकारी शिक्षा की घटती गुणवत्ता और लोकप्रियता को पुनःप्राप्त करने के लिए एक शिक्षक के रूप में स्वयं को अधिक समर्थ और समर्पित बनाना। हमें एक शिक्षक के रूप में समाज में खोते जा रहे विश्वास को पुनः बहाल करने के लिए काम करना होगा।
पहले मोर्चे की लड़ाई को हम मजबूती से लड़ सकें। पूरे समाज का सहयोग प्राप्त कर सकें इसके लिए हमें दूसरे मोर्चे पर सक्रियता से काम करना होगा। अपने विद्यालयों के माहौल को अधिक रचनात्मक और आकर्षक बनाना होगा। व्यवस्थाजनित सृजनशीलता विरोधी माहौल को तोड़ना होगा। बच्चों में सृजनशीलता के विकास के लिए हमें अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। हमें तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करना होगा। साथ ही तमाम विद्यालयों में किए जा रहे सृजनात्मक कार्यों को समाज के सामने लाना होगा। इसी उद्देश्य से हमने अपने विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज, देवलथल में एक छोटी सी पहल की।
बच्चों की सृजनात्मकता को मंच देने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए हमने ‘दीवार पत्रिका’ के प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया। यह विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला पाक्षिक आयोजन है। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है विद्यालय की दीवार में लगाया जाता है। इसमें बच्चों द्वारा तैयार की गई कहानी, कविता, लेख ,संस्मरण, चुटकुलों, पहेलियों, समाचार, वर्ग पहेली, सामान्य ज्ञान संबंधी तथ्य, चित्र, कार्टून आदि को एक कागज में सुलेख में लिखकर एक लंबे आदमकद चार्ट में चिपकाया जाता है। संपादन कार्य पूरी तरह बच्चों द्वारा किया जाता है। बच्चों का एक संपादक मंडल बनाया गया है, जो सामग्री का संकलन और चयन करते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए देश भर से निकलने वाली विभिन्न बाल पत्रिकाएं दी जाती हैं ताकि वे अनुभव ले सकें। उन पत्रिकाओं से भी अपनी दीवार पत्रिका के लिए उपयोगी सामग्री लेते हैं। बच्चों को दीवार पत्रिका की प्रतीक्षा रहती है। छपने के लिए बच्चों में उत्सुकता बढ़ने लगी। बच्चे सामग्री को पढ़कर प्रतिक्रिया देने लगे। साहित्य की विभिन्न विधाओं और पत्रकारिता की बारीकियों को जानने-समझने लगे।
दीवार पत्रिका को प्रारंभ करते हुए कुछ कठिनाइयां आईं। बार-बार कहने पर भी बच्चों ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। बच्चों को स्वयं रचना तैयार करना कठिन काम लगता था। लेकिन, उन्हें निरंतर प्रोत्साहित किया गया। पढ़ने के लिए बाल साहित्य दिया गया। उसके महत्व से उन्हें अवगत कराया गया। एक-दो अंक तैयार कर उनके सामने प्रस्तुत किए गए। हिंदी शिक्षण के दौरान ही उन्हें अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित किया गया। छोटी-छोटी कविताएं, कहानियां, निबंध, लेख, यात्रा वृतांत, जीवन-प्रसंग आदि तैयार करवाए गए। समय-समय पर विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और आसपास की घटनाओं की रिपोर्टिंग करवाई गई। उनमें से बेहतर रचनाओं को दीवार पत्रिका में लगाया जाने लगा। इसके लिए मासिक परीक्षाओं तक का भी उपयोग किया गया। हिंदी की परीक्षा में बच्चों अपने अनुभव पर कुछ लिखने को कहा गया। एक बार कक्षा नौ के बच्चों से कहा गया कि अपने जीवन के किसी ऐसे प्रसंग को लिखें जब उन्हें बहुत खुशी हुई या रोना आया हो। बच्चों ने बेहद रोचक प्रसंग लिखे। इससे यह भी जानने को मिला कि बच्चे अपने आसपास को कैसे देखते हैं ? अपने बड़ों के प्रति क्या सोचते हैं ? उन्हें जीवन में कौन सी घटना प्रसन्नता देती है और कौनसी दुःख पहुंचाती है ?
कक्षा में दो लाइन पड़ती थी भारी… 3-3 पन्नों में लिख डाले संस्मरण
सबसे रोचक तथ्य जो सामने आया कि जो बच्चे आमतौर से कक्षा में दो-चार पंक्तियां भी नहीं लिख पाते थे, उन्होंने दो-दो ,तीन-तीन पृष्ठों में अपने संस्मरण लिख डाले। कुछ संस्मरण को दीवार पत्रिका में स्थान दिया गया। इससे हमारा विश्वास बढ़ा कि यदि बच्चों को अवसर दिए जाएं तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। शुरुआत में दो-चार बच्चे की ही दीवार पत्रिका में भागीदारी होती थी। फिर निर्णय लिया गया कि बच्चों का एक समूह तैयार किया जाए। 6 से 12 तक की प्रत्येक कक्षा से ऐसे बच्चों का चयन किया गया जो बेहतर माने जाते थे। कुछ ऐसे बच्चों को भी चुना गया जिनका हस्तलेख बहुत सुंदर था या चित्रकला में अच्छा करते थे। 30-35 बच्चों का ऐसा एक समूह गठित किया गया जिसे ‘बाल बौद्धिक प्रकोष्ठ’ नाम दिया गया। इनकी बैठकें कराईं। जिसका संचालन बच्चों द्वारा ही किया गया। बच्चों ने आम सहमति और रुचि के अनुकूल दीवार पत्रिका के लिए दस सदस्यीय संपादक मंडल का चयन किया गया। भूमिकाओं का वितरण भी किया। अब सामग्री संकलन-चयन से लेकर चार्ट में चिपका कर उसे पत्रिका का स्वरूप प्रदान करने की सारी जिम्मेदारी यही संपादक मंडल करता है।
पैदा हुई सामूहिकता की भावना
इस कार्य से एक और लाभ हुआ। बच्चों में सामूहिकता की भावना पैदा हुई। ये बैठकर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। समस्याओं को एक-दूसरे के साथ बांटते हैं । रणनीति बनाते हैं। पढ़ने-लिखने में एक-दूसरे की मदद करते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापकों से मिलते हैं। इनका लक्ष्य है कि विद्यालय तथा अपने गांव-पड़ोस का वातावरण शैक्षिक तथा रचनात्मक बनाया जाए। बच्चों में रचनात्मक लेखन के विकास के लिए विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। लेकिन, हमारा मानना है कि उसकी कुछ सीमाएं हैं । अधिक खर्चीली होने के कारण उसका वर्ष में एक से अधिक अंक निकालना संभव नहीं है। जहां छात्र संख्या कम है वहां एक बार निकाल पाना भी संभव नहीं हो पाता। इसमें संपादन से लेकर प्रकाशन में बच्चों की अपेक्षा अध्यापकों की सक्रियता और भागीदारी ही अधिक रहती है, जिससे बच्चों को बहुत अधिक कुछ कर पाने तथा सीखने का अवसर नहीं मिल पाता है। लिखने का अवसर भी वर्ष में एक ही बार मिल पाता है। अतः लेखन कौशल के विकास एवं बच्चों की अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने की दृष्टि से इसे बहुत उपयोगी नहीं कहा जा सकता है। अगर हर स्कूल में विद्यालय पत्रिका के साथ दीवार पत्रिका भी निकाली जाए तो दोनों का महत्व बढ़ जाएगा।
किताब कौथिग … जगा रहा रचनात्मकता और साहित्य की अलख
दीवार पत्रिका का यह अभिनव प्रयोग केवल राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में ही नहीं पिथौरागढ़ जिले के एक दूरस्थ विद्यालय क.पू.मा.वि. नाचनी में रचनात्मक शिक्षक मंडल के राज्य सचिव राजीव जोशी द्वारा भी किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रयोग को प्रारंभ करने से पूर्व एक पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। जिसमें बच्चों को आवश्यक जानकारी देने के साथ ही लेखन कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से रोचक गतिविधियां करवाई गई। प्रसन्नता की बात है कि वहां भी यह प्रयोग सफल है। हमारा मानना है कि यह प्रयोग हर विद्यालय में किया जाना चाहिए। यह न केवल बच्चों की भाषायी दक्षता ,अध्ययन की प्रवृत्ति और सृजनशीलता बढ़ाने में सहायक है बल्कि विद्यालयों में अनुशासन की समस्या को सुलझाने में भी एक हद तक मददगार है। रचनात्मक शिक्षक मंडल के सदस्यों को इसे एक अभियान की तरह लेना चाहिए। इससे पर्याप्त अनुभवों को रचनात्मक शिक्षक मंडल के आगामी सम्मेलनों में आपस में बांटा जाना चाहिए ताकि इसको अधिक उपयोगी और प्रभावकारी बनाया जा सके। (लेखक प्रख्यात कवि एवं लेखक और शिक्षाविद हैं।)