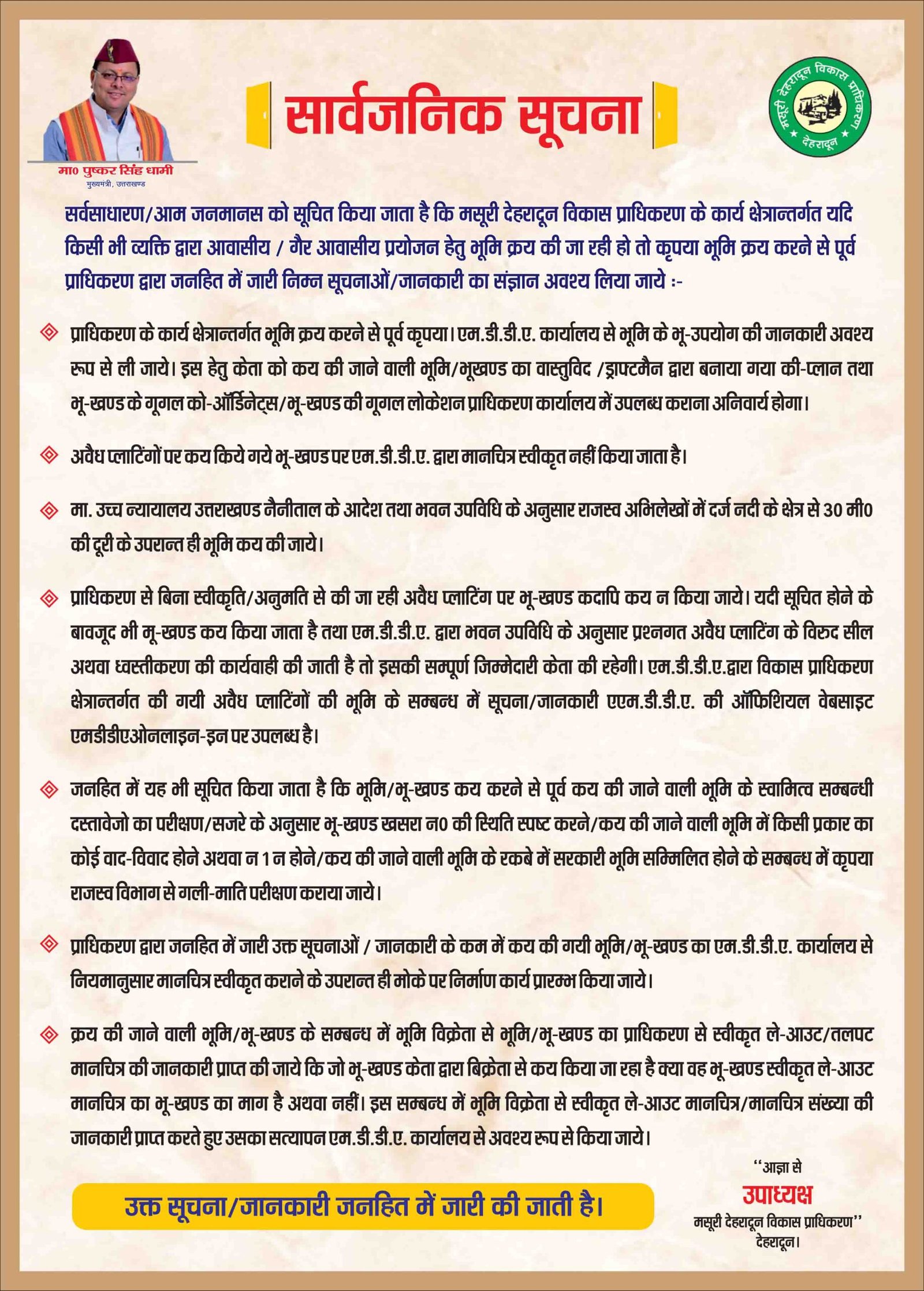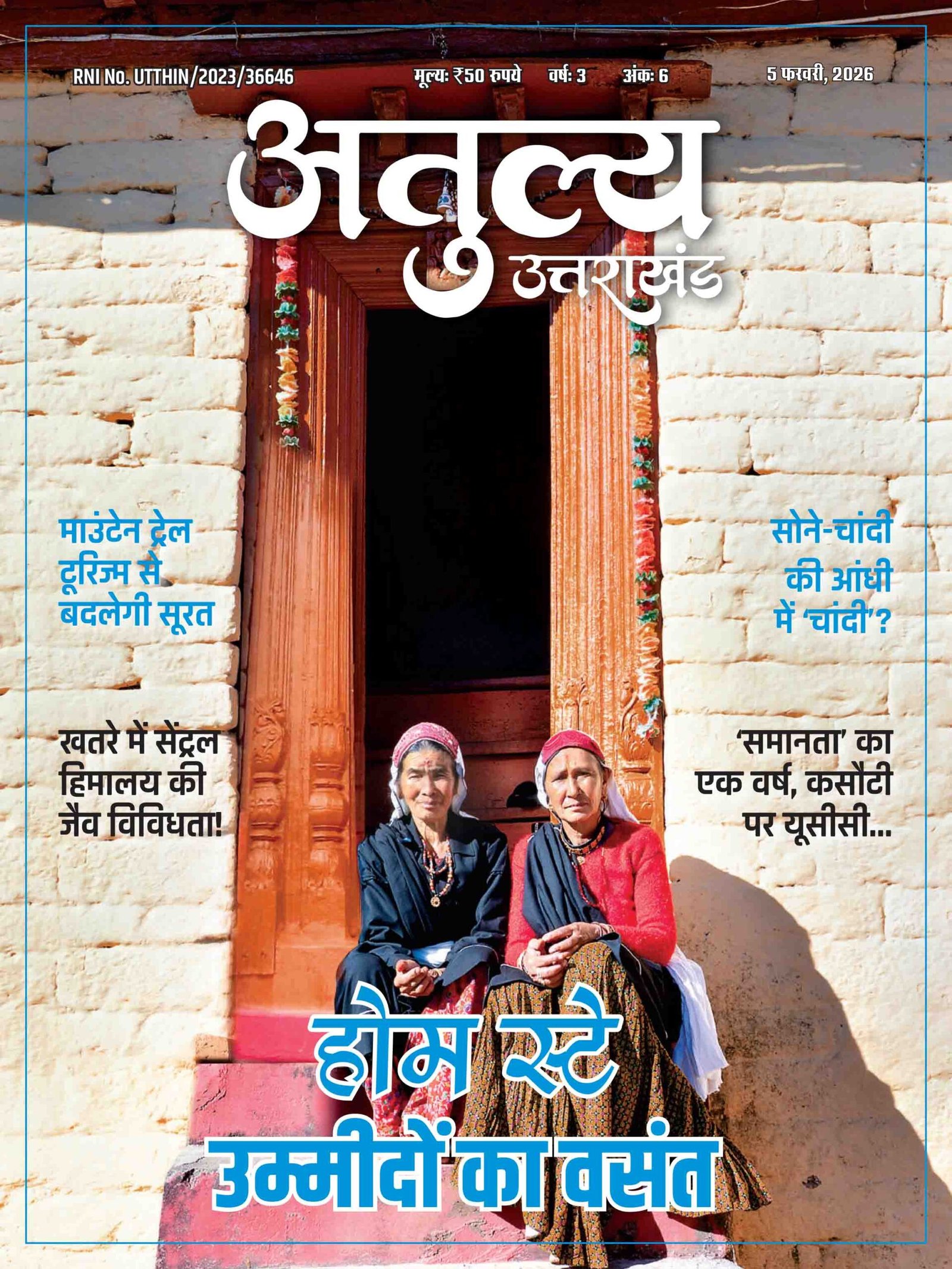- डा. तेजपाल सिंह बिष्ट/डा. लक्ष्मी रावत
कृषि एवं बागवानी के अतिरिक्त उत्तराखंड की वन संपदा भी इसके लिए वरदान है। पर्यावरण, मृदा संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के परिपेक्ष्य में भी इनका बहुत महत्व है। परंतु आज कई प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से उपजी वनाग्नि व जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थिकी तंत्र में विपरीत बदलाव आ रहे हैं। इन बदलावों से प्रदेश की जैव विविधता परोक्ष रूप से प्रभावित हो रही है जो राज्य के समक्ष भविष्य में भयावह संकट उत्पन्न कर सकती है। उत्तराखंड में आज भी पुरानी जीविका कृषि पद्धति प्रचलित है जिसे आम बोलचाल में व्यावहारिक कृषि पद्धति कहा जाता है। जिसमें कृषि सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जा रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में अभी तक कृषि को वाणिज्य से नहीं जोड़ा गया है। मुख्य फसलों के साथ-साथ फल-फूल, औषधीय वनस्पति आदि से वाणिज्य को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। कृषि एवं वाणिज्य के ढृढ़ गठबंधन से ही क्षेत्र के लोगों के आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसरों में सुधार लाया जा सकता है। तभी हम युवाओं में पलायन की प्रवृत्ति को भी रोक पाएंगे। पर्वतीय कृषकों के लिए ऐसे मॉडल का निर्माण एवं समावेश करने की आवश्यकता है, जिससे कृषक अपने उत्प
व्यावसायिक-वैज्ञानिक खेती का जमाना
राज्य में बागवानी के लिए उभरती चुनौतियां बहुआयामी और आपस में जुड़ी हुई हैं। जिससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यदि हमें उत्तराखंड में खेती के स्वरूप को बदलना है तो व्यावहारिक खेती से वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती की तरफ आना पड़ेगा। क्षेत्र विशेष की जलवायु और स्थलाकृति के अनुरूप कृषि बागवानी के ऐसे मॉडल स्थापित करने पड़ेंगे जिससे राज्य के कृषक-बागवानी करने वालों को सरकारी कर्मचारियों की तरह मासिक आय मिल सके। राज्य की सरकारी नीतियां और सहायता प्रणालियां अक्सर बागवानों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त साबित हुई हैं। जिसका मुख्य कारण आज भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जलवायु और स्थलाकृति स्थितियों के अनुरूप बागवानी अनुसंधान और विस्तार सेवाओं की कमी है।
राज्य में कृषक/बागवानी द्वारा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जबकि, उत्पादन बढ़ाने के साथ ही यह भी बेहद जरूरी है कि मिट्टी एवं जल संरक्षण की ओर भी ध्यान दिया जाए। किसी भी क्षेत्र के उत्पादन का मूल उसकी मृदा का उत्पादन एवं जल उपलब्धता है। कृषि एवं बागवानी जैसी पद्धतियों से मृदा में कार्बन की मात्रा एवं उसके संतुलन को बढ़ाकर उसके उपजाऊपन को बढाया जाना चाहिए। साथ ही जैविक खेती से भी यहां के किसानों के लिए कम लागत एवं अधिक लाभ के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। भरपूर जल स्त्रोत होने के बाद भी उचित जल प्रबंधन तकनीक न होने एवं उनके उपेक्षाकृत कम प्रसार के कारण प्रदेश में अधिकतर कृषक वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं। इन समस्याओं पर ध्यान देना अतिआवश्यक है। पर्वतीय भूभाग में जितनी जैव विविधता है, उतनी मैदानी क्षेत्रों में नहीं है। उत्तराखंड में जैव विविधता में भी खाद्य-पदार्थ उपलब्ध कराने वाले पौधों की अधिकता है। इस क्षेत्र में बारानाजा खेती जिसके अंतर्गत मंडुवे, झंगोरे के साथ अन्य कई फसलें जैसे विभिन्न दालें, कुट्टू, रामदाना, चैलाई इत्यादि की खेती बहुत प्रचलित हैं। साथ ही कई खेती फसलें एवं औषधीय पौधें हैं जिसकी उपलब्धता दूसरी जगहों पर नहीं है। अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण इनकी मांग देश-विदेश में भी बढ़ने लगी है।
कृषि का मौजूदा हाल
कृषि क्षेत्र का राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 22.4 प्रतिशत का योगदान है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 13.52 प्रतिशत भू-भाग पर फसलों की शुद्ध बुवाई की जाती है। राज्य के पर्वतीय आंचल में अधिकांश कृषि कार्य के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पडता है। घाटी एवं मैदानी क्षेत्रों में स्थानीय नदियों एवं नालों के पानी को कच्चे गूल एवं नहरों की सहायता से खेतों तक पहुंचाया जाता है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 12 प्रतिशत भाग ही कृषि के अंतर्गत है। कृषि क्षेत्र का 54 प्रतिशत पर्वतीय तथा 46 प्रतिशत मैदानी है। पर्वतीय कृषि वर्षा आधारित है, इसका केवल 19 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है। प्रदेश में 91 प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमांत जोत वाले है क्योंकि राज्य में कृषि जोत का औसत आकार लगभग 0.98 हेक्टेयर है। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता कम है।
पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतयः साल में दो फसलें ली जाती हैं। जबकि घाटी या मैदानी क्षेत्रों में तीन फसलें ली जाती हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतयः मिश्रित खेती का प्रचलन है जिस कारण पर्वतीय क्षेत्रों को बारानाजा क्षेत्र भी कहा जाता है। राज्य में सबसे अधिक गेहूं, चावल, मक्का, रागी, झंगोरा, चैलाई आदि की खेती की जाती है परंतु फसलों की उत्पादकता अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। राज्य में कुछ बहुमूल्य फसलें जैसे- कुट्टू, बथूवा, फाफरा, कालाभट्ट, तोर, गहत, नौरंगी, एडजुकी बीन, सूंटा (लोबिया), भंगजीरा, तिल, च्यूरा, जंबू, काला जीरा, झूला, जख्या, दालचीनी, भांग आदि फसलों की भी खेती की जाती है।
देवभूमि में कृषि-बागबानी की स्थिति
- कृषि क्षेत्र का राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 22.4 प्रतिशत का योगदान।
- राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 13.52 प्रतिशत भू-भाग पर फसलों की होती है बुवाई।
- भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 12 प्रतिशत भाग ही कृषि के अंतर्गत।
कृषि क्षेत्र
- 54 प्रतिशत पर्वतीय
- 46 प्रतिशत मैदानी
- 86 प्रतिशत के करीब उत्तराखंड की जनसंख्या कृषि पर निर्भर
बागवानी का गणित भी समझिये
- राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 2.79 लाख हेक्टेयर पर की जाती है बागवानी।
- हर साल लगभग 2300 करोड़ रुपये की आय राज्य को प्राप्त होती है बागवानी से।
- कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान बागवानी का।
- देश में पहला पायदान – नाशपाती, आडू, पूलम एवं खुबानी उत्पादन
- अखरोट उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड
- सेब उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है ये हिमालयी राज्य
मसाला फसलों की खेती
1460 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है मसाला फसलों की खेती। प्रति इकाई क्षेत्रफल में मसालों की उत्पादकता में उत्तराखंड का देश में पहला स्थान।
छोटे और सीमांत किसानों के लिए एकीकृत खेती ही लाभकारी रास्ता है, जिसमें खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और बागवानी को जोड़ना होगा।
– शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, भारत
बागवानी की स्थिति
वर्तमान में बागवानी की दशा ठीक कही जा सकती है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन, इस क्षेत्र में अब भी अपार संभावनाएं है। भौगोलिक स्थितियां और जलवायु औद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल है। राज्य के पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र सेब, नाशपाती, प्लम, अखरोट, बादाम, खुबानी, आडू, कीवी एवं बेमौसमी सब्जियों, मसाला, पुष्प आदि के उत्पादन के लिए अनुकूल है। वहीं, दूसरी ओर प्रदेश के उक्त जिलों की घाटियां, उधमसिंहनगर एवं हरिद्वार तथा नैनीताल, देहरादून के मैदानी क्षेत्र समशीतोष्ण फलों जैसे आम, अमरुद, लीची, आंवला, नीबू प्रजाति के फलों, मौसमी सब्जियों, मसालों एवं फूलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जड़ी-बूटी, सगंध पौध, मशरूम, मधु (शहद), रेशम तथा चाय उत्पादन की भी अपार संभावनाएं हैं। बेमौसमी सब्जियों जैसे शिमला मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी फ्रैंच बीन, मटर तथा टमाटर के उत्पादन से किसान आय और रोजगार के नए द्वार खोल रहे हैं।

कृषि-बागवानी की संभावनाएं
प्रदेश में भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के आधार पर कृषि को दो भागों में बांटा जा सकता है। वे संसाधन क्षेत्र जहां सिंचाई की उत्तम सुविधा, उपजाऊ भूमि तथा बड़ी जोते हैं, वहां व्यापक स्तर पर कृषि यंत्रों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। इन क्षत्रों में कृषि का विविधीकरण तेजी से होता जा रहा है। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों जो कि असिंचित तथा वर्षा पर पूर्णतः आश्रित है। ऐसे कृषि क्षेत्र समुद्र सतह से 1500 मीटर से 2500 मीटर तक स्थित है। जहां अधिकाशतः लघु तथा सीमांत कृषक हैं, वहां आज भी कृषि विकास की किरण नही पहुंच पाई है। इन क्षेत्रों को चुनौती के रूप में लेते हुए आवश्यक है कि कृषकों को जल संरक्षण, उन्नतशील बीज, समय से खाद तथा उर्वरक की उपलब्धता एवं पर्यावरण आधारित फसल सुरक्षा की विभिन्न विधियों की तकनीकी जानकारी सुलभ हो ताकि उत्पादकता में वृद्धि कर कृषक अपनी आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुदृढ़ कर सकें।
जैव विविधता का भंडार
राज्य में कृषि जैव-विविधता का विशाल भंडार है। यहां पर एक ही फसल की विभिन्न प्रजातियां या स्थानीय किस्में उपलब्ध हैं। जिसके फलस्वरुप यहां के किसान कुल मिलाकर 100 से अधिक फसलों को उगाते हैं जो कि जैव-विविधता का एक उत्तम उदाहरण है। परंपरागत फसलें जो कि जलवायु परिवर्तन के दौर में भी अच्छा उत्पादन करती हैं तथा भविष्य में पर्यावरण के बदलाव में भी उत्पादन की महत्वपूर्ण क्षमता रखती हैं। इन फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसानों को यह समझाने की जरूरत है कि वह इससे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कुल कृषि क्षेत्रफल का अधिकांश क्षेत्रफल वर्षा आधारित है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल संचय एवं उसके उपयोग से अन्य योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश के किसानों को अधिक लाभ दिया जा सकता है। राज्य की विषम कृषि जलवायु परिस्थिति यहां के किसानों को बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए अवसर प्रदान करती है। वहीं, फलों की खेती करने वाले कृषक साथ में मौनपालन कर सकते हैं। जिससे कि दोहरे लाभ जैसे कि फसलों में मौनपालन द्वारा परागण बढा कर फलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। एवं मौनपालन में नवीनतम तकनीकी अपनाकर जैविक एव औषधीय गुणों से संपन्न गुणवत्तायुक्त मधु का उत्पादन एवं निर्यात कर विदेशी पूंजी अर्जित करने की अपार संभावनाएं हैं।
वर्तमान में उत्तराखंड में औद्याानिकी विकास की समस्त योजनाएं ‘कलस्टर अवधारणा’ के आधार पर क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे अधिक मात्रा में फसल विशेष का उत्पादन कर विपणन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा सके। इससे उन क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर न सिर्फ पलायन को रोका जा सकता है, साथ ही उत्पादन में वृद्धि कर किसानों का आर्थिक जीवन स्तर भी सुधारा जा सकता है। प्रदेश के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में बागवानी फसलों को दिए जाने वाले महत्व से कुछ नए जागरूकता आई है। इन फसलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है तथा उत्पादकों को इन फसलों से बेहतर आमदनी होने लगी है। बागवानी फसलों की निरंतर बढ़ती मांग के सापेक्ष आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन फसलों के क्षेत्रफल में व्यापक स्तर पर विस्तार ही उत्पादकता में वृद्धि हो तथा कम लाभदायी फसलों के स्थान पर बागवानी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाए। उत्तराखंड राज्य की आर्थिक व्यवस्था में बागवानी का विशेष योगदान है।
प्रदेश में बागवानी मिशन योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2003-04 से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से औद्यानिकी के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत बागवानी मिशन योजना में समाहित किया गया है। इस योजना के तहत गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का उत्पादन, फल, सब्जी, मसाला व पुष्प क्षेत्रफल विस्तार, पुराने बगीचों का जीर्णोंद्वार, मशरूम उत्पादन, मौनपालन, जल स्रोतों को सृजन, संरक्षित खेती, जैविक खेती, औद्याानिकी यंत्रीकरण, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, विपणन एवं प्रसंस्करण संबंधी अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना के साथ-साथ प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम सम्मिलित हैं।
पर्वतीय क्षेत्र में अपार संभावनाएं
पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि वानिकी की भी अपार संभावनाएं हैं। यहां अधिकतर भू-भाग में वन है। कृषि कार्य एवं पशुपालन का कार्य वनों पर अधिक निर्भर करता है। खेतों की मेड़ों पर बहुउद्देश्यीय पौधों की रोपाई करके लकड़ी, चारा एवं ईंधन तथा खेतों से फसलें प्राप्त कर सकते हैं। फलों के बगीचे में पौधों से पौधों के बीच उचित दूरी रखकर अंतर फसल के रूप में अनाज फसलें, सब्जियों, फूलों आदि की खेती करके प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक से अधिक लाभ कमा सकते है। वर्षा आधरित खेती में मेड़ों पर फलदार वृक्ष जैसे कि आडू, पूलम, खुबानी, अखरोट, नाशपाती एवं सेब के पौधे या फिर चारे वाले पौधे जैसे कि भीमल, खड़ीक, तिमला आदि पौधों की रोपाई करके भूमि कटान को रोका जा सकता है तथा साथ ही साथ फसलों या सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरुप पशु के लिए चारा और फल तथा फसलों का उत्पादन अधिक किया जा सकता है।
कृषि-बागवानी से प्रति कृषक आय
उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 86 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी एवं 14 प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है। राज्य की जनसंख्या लगभग 1.01 करोड़ है। उत्तराखंड में किसानों और ग्रामीण लोगों की आय कृषि अर्थव्यवस्था और प्रदेश के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हालांकि, किसानों और ग्रामीण परिवारों के बीच आय का स्तर कई कारणों से व्यापक रूप से भिन्न होता है। जिसमें भूमि का आकार, प्रौद्योगिकी तक पहुंच, सरकारी सहायता और बाजार की स्थितियां शामिल हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में में एक किसान की औसत मासिक आय सभी स्रोतों से लगभग 5000 से 10000 रुपये होने का अनुमान है। हालांकि, यह आंकड़ा क्षेत्रों, फसलों के प्रकार और भूमि जोत के आकार के अनुसार काफी भिन्न होता है। छोटे और सीमांत किसान बड़े पैमाने के किसानों की तुलना में बहुत कम कमाते हैं।
आय के स्रोत
• कृषि गतिविधियां: कृषि ग्रामीण आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है। छोटे और सीमांत किसान फसल की खेती और पशुधन, डेयरी फॉर्मिंग, मुर्गी पालन आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों जैसे आय के मिश्रित स्रोत पर निर्भर हैं।
• गैर-कृषि आय: कई ग्रामीण लोग गैर-कृषि आय स्रोतों जैसे ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, निर्माण, सेवा क्षेत्र और मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं पर भी निर्भर हैं, जो साल में 100 दिनों के लिए गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती हैं।
• सरकारी पहल: पीएम-किसान योजना किसानों को सालाना 6000 रुपये प्रदान करती है। अन्य पहलों में बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि के लिए सब्सिडी शामिल हैं।

क्या है बागवानी-केंद्रित एकीकृत कृषि मॉडल ?
बागवानी-केंद्रित एकीकृत कृषि मॉडल किसानों की आय, उत्पादन बढ़ाने का प्रभावी विकल्प माना जा रहा है। इसमें बागवानी फसलें (फल, सब्जियां, फूल आदि) मुख्य घटक होती हैं। अन्य कृषि गतिविधियां (पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी आदि) उनके साथ मिलकर काम करती हैं। इस प्रणाली में दो या दो से अधिक घटकों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है ताकि एक घटक के समायोजन से दूसरे घटक की लागत में कमी हो। उत्पादन में वद्धि हो। पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहे, साथ ही साथ किसानों को प्रतिदिन या महीने भर आमदनी प्राप्त होती रहे। इस मॉडल में किसान बागवानी फसलों के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी एवं अन्य संबंधित गतिविधियों जैसे जैविक खेती, सघन रोपण, संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण को भी शामिल कर सकते हैं। ताकि सभी एक-दूसरे के लिए पूरक बनें जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। पशुधन आधारित बागवानी-केंद्रित एकीकृत कृषि प्रणाली एक समग्र कृषि दृष्टिकोण है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
उदाहरण के लिए, एक किसान बागवानी फसलों के साथ-साथ, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती कर सकता है। पशुधन से प्राप्त खाद का उपयोग बागवानी फसलों के लिए उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। बागवानी फसलों के अवशेषों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। इसी तरह, मछली पालन के लिए बानाये गए तालाबों के किनारे फलदार पेड़ लगाए जा सकते हैं, तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। इसी तरह, मधुमक्खियां परागण में मदद करती हैं और मशरूम की खेती के लिए अपशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है। अतीत में, हमने चुनौतियों का सामना किया है और दिखाया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली कृषि लाखों लोगों के लिए भोजन उगाना संभव बना सकती है। जैविक खेती, सघन रोपण, संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण जैसी आधुनिक तकनीकों की संरचना एवं क्रिर्यान्वयन फसल की पैदावार को अधिकतम करने के लिए शामिल है। उत्तराखण्ड भारत का पहला और एकमात्र प्रांत है जिसने जैविक खेती नीति विकसित की है। जैविक फसल के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं।
एक खेत से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने को ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। जब हम किसी एक क्रॉप पर निर्भर होते हैं तो उसके खराब होने की दशा में किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। वह परेशान हो जाता है। इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग में आपके पास कई विकल्प होते हैं। अगर कोई एक फसल फायदा नहीं देती है तो दूसरी फसल उसकी भरपाई कर देती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इंटीग्रेटेड मॉडल की सख्त जरूरत है। इंटीग्रेटेड मॉडल में हार्टीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। बागबानी करने वालों को सब्जियों पर फोकस करना चाहिए। इससे उन्हें नियमित आमदनी होने लगेगी। अदरक और हल्दी की खेती खूब सफल होगी, क्योंकि इन्हें छायादार माहौल की जरूरत होती है। साथ ही अन्य सब्जियों की खेती पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे किसानों की नियमित आय होने लगेगी। दरअसल, बागबानी में सीजन-सीजन पैसे मिलते हैं। ऐसे में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों को ऐसी पूरक फसलों का चयन करना चाहिए जिससे वह साल भर क्रॉपिंग ले सकें। किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई स्कीमें हैं। कृषि विभाग की बायोडायवर्सिटी योजना, डेयरी और अन्य योजना का भी लाभ किसान ले
– डा. सतेंद्र नरवरिया, उपनिदेशक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

सोलर फेंसिंग के लिए सरकारी मदद की दरकार
• इंटीग्रेटेड प्रणाली में सबसे बड़ी चुनौती जंगली जानवरों का उत्पात है। खुशीराम डबराल कहते हैं, सरकार को खेतों में बाड़ लगाने में सहयोग करना चाहिए। सरकार अब भी सब्सिडी दे रही है लेकिन उसे बढ़ाकर किसानों की मदद की जा सकती है। हमने तो अपने खेत को सोलर तार से सुरक्षित कर लिया है। लेकिन, छोटे किसानों के पास इतनी पूंजी नहीं होती।
• कौशल रावत भी बताते हैं कि सरकार को इस दिशा में सब्सिडी बढ़ानी चाहिए। जब खेत सुरक्षित होंगे तो किसान कुछ न कुछ करने को सोचेंगे। कोई भी पहाड़ी दिल्ली में जाकर 15-20 हजार की नौकरी नहीं करना चाहता। खासकर जिसके पास 10-15 नाली खेत हैं, क्योंकि वह दिल्ली से ज्यादा पैसे इन खेतों से पैदा कर लेगा। लेकिन, इतने खेत को सोलर फेसिंग से सुरक्षित करना उसके बस की बात नहीं है। सरकार इनकी मदद करे तो खेती की दशा में काफी सुधार हो जाए।

चकबंदी समय की मांग

• राज्य में कृषि योग्य बेकार भूमि 32886 हेक्टेयर बढ़ चुकी है। यह 2019-20 में 329564 हेक्टेयर थी। 2022-23 में 362450 हो चुकी है। वहीं, वास्तविक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच 72,490 हेक्टेयर भूमि पर खेती घट गई।
• राज्य में लंबे समय से भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। ऐच्छिक चकबंदी की योजना भी प्रभाव नहीं छोड़ पाई। नतीजा यह है कि पहाड़ में जिस भूमि पर फसलें उगाई जा सकती थीं, वहां झाडि़यां और पेड़ उग गए हैं। खेती उजाड़ और बर्बाद हो चुकी है। वन और राजस्व भूमि की स्पष्टता न होने से भी कृषि में दिक्कत आती है।
• प्रगतिशील किसान कौशल रावत कहते हैं, सरकार खाली पड़ी उजाड़ भूमि पर खेती करने की छूट दे। हिमाचल में ऐसा करने से अच्छे नतीजे मिले हैं। पढ़े-लिखे युवा भी खेती करना चाहते हैं। सरकार भी नीति बना रही है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब भूमि आसानी से मिलेगी। पहाड़ में खेती गोल खातों में उलझी हुई है। चकबंदी के अभाव में पहाड़ में खेती बिखरी और असुरक्षित है। सामूहिक खेती को अपनाकर जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और जोखिम भी घटेगा। राज्य में 15700 से अधिक राजस्व गांव हैं। केंद्र की नीति के तहत 2030 तक देश के हर राजस्व गांव में भूमि बंदोबस्त होना है।
हम सबको पता है कि कैसे फॉर्मिंग कराई जाए। लेकिन, दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीति नियंता इसपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड का लगभग 60 प्रतिशत ड्राई एरिया है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी फसल करें, जो हमारे अनुकूल हैं। मेरा 17 साल का अनुभव है। इसलिए हम सफल हैं। लेकिन, बाकी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेब की खेती के लिए प्रोत्साहित तो कर रहे हैं। लेकिन, यह नहीं बता रहे हैं कि उसकी देखभाल कैसे करें। मुझे लगता है कि तंत्र उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, जैसे उसे करना चाहिए। हमारी मिट्टी हर्बल के लिए मुफीद है। लेकिन, इसके लिए भी नीतियां सही नहीं हैं। हमने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने भी यह मुद्दा उठाया। आज मैं दो करोड़ रुपये कमा रहा हूं तो उसके लिए हमने जो किया वह छोटे-मंझोले किसानों के बस की बात नहीं है। यहां सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। हमें आधुनिक कृषि के साथ-साथ पारंपरिक कृषि ज्ञान को भी साथ लेकर चलना चाहिए।
उत्तराखंड का लगभग 60 प्रतिशत ड्राई एरिया है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी फसल करें, जो हमारे अनुकूल हैं। हम हर्बल बेस्ड इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग करते हैं, इसलिए शायद हम सफल हैं। हम एरोमा टूरिज्म पर काम कर रहे हैं। लेकिन, दूसरे किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में जंगली जानवर खेती के लिए चुनौती बन गए हैं। हॉर्टीकल्चर की बात करें तो किसानों को प्रोत्साहित तो किया जा रहा है लेकिन यह बताना भी जरूरी है कि फलदार पेड़ों की देखभाल कैसे करें। हमारी मिट्टी हर्बल के लिए मुफीद है। लेकिन, इसके लिए प्रभावी नीतियों पर काम करना होगा। हमने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने भी यह मुद्दा उठाया है। आज मैं दो करोड़ रुपये तक कमा सकता हूं, उसके लिए हमने जो मॉडल विकसित किया वह हर छोटे-मंझोले किसान के करना आसान नहीं है। छोटे किसानों को सरकार की मदद की जरूरत है। हमें पारंपरिक कृषि ज्ञान को भी साथ लेकर चलना चाहिए।
(डा. तेजपाल सिंह बिष्ट हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के औद्यानिकी विभाग और डा. लक्ष्मी रावत, कृषि महाविद्यालय, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरा से संबंद्ध हैं।)