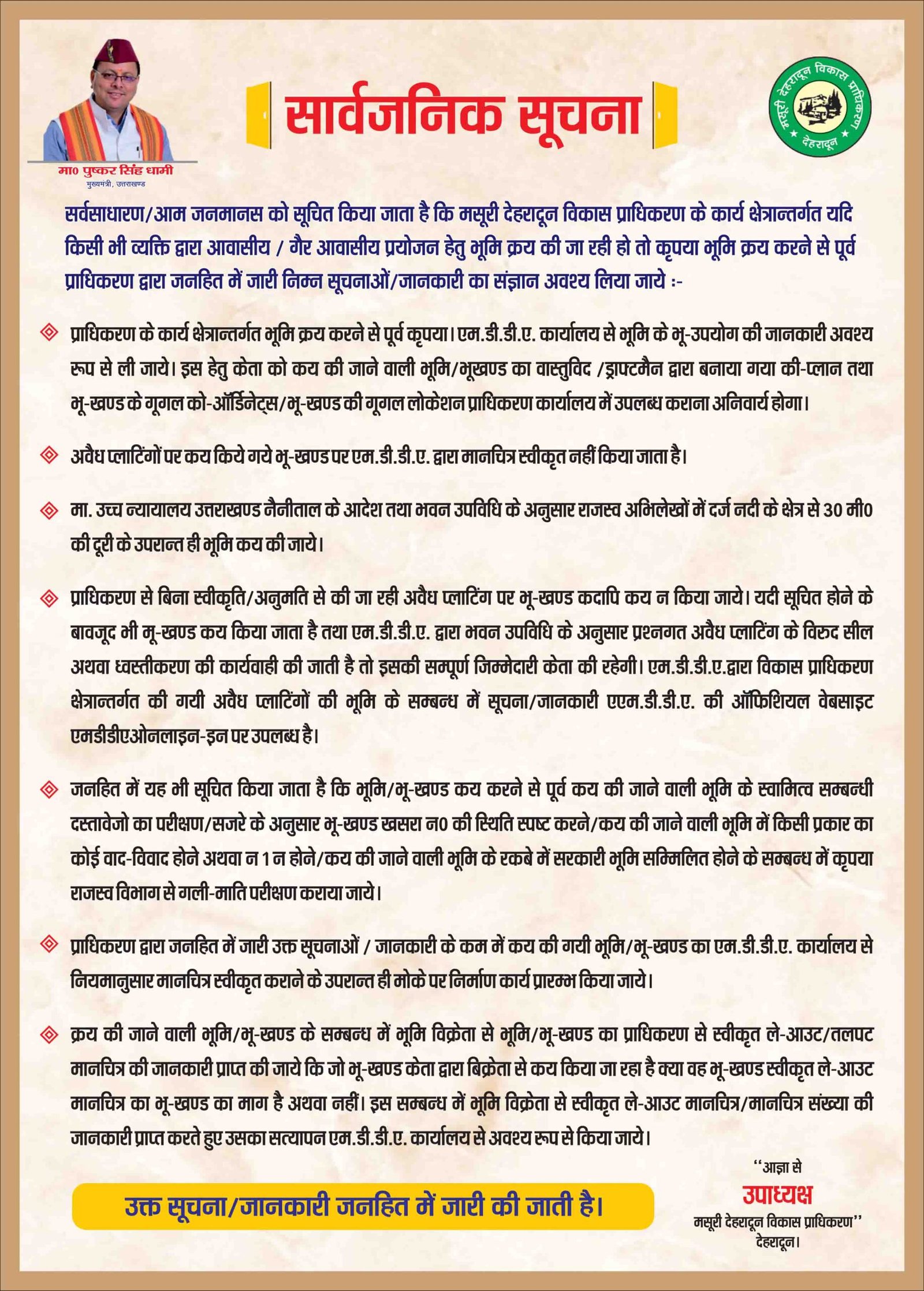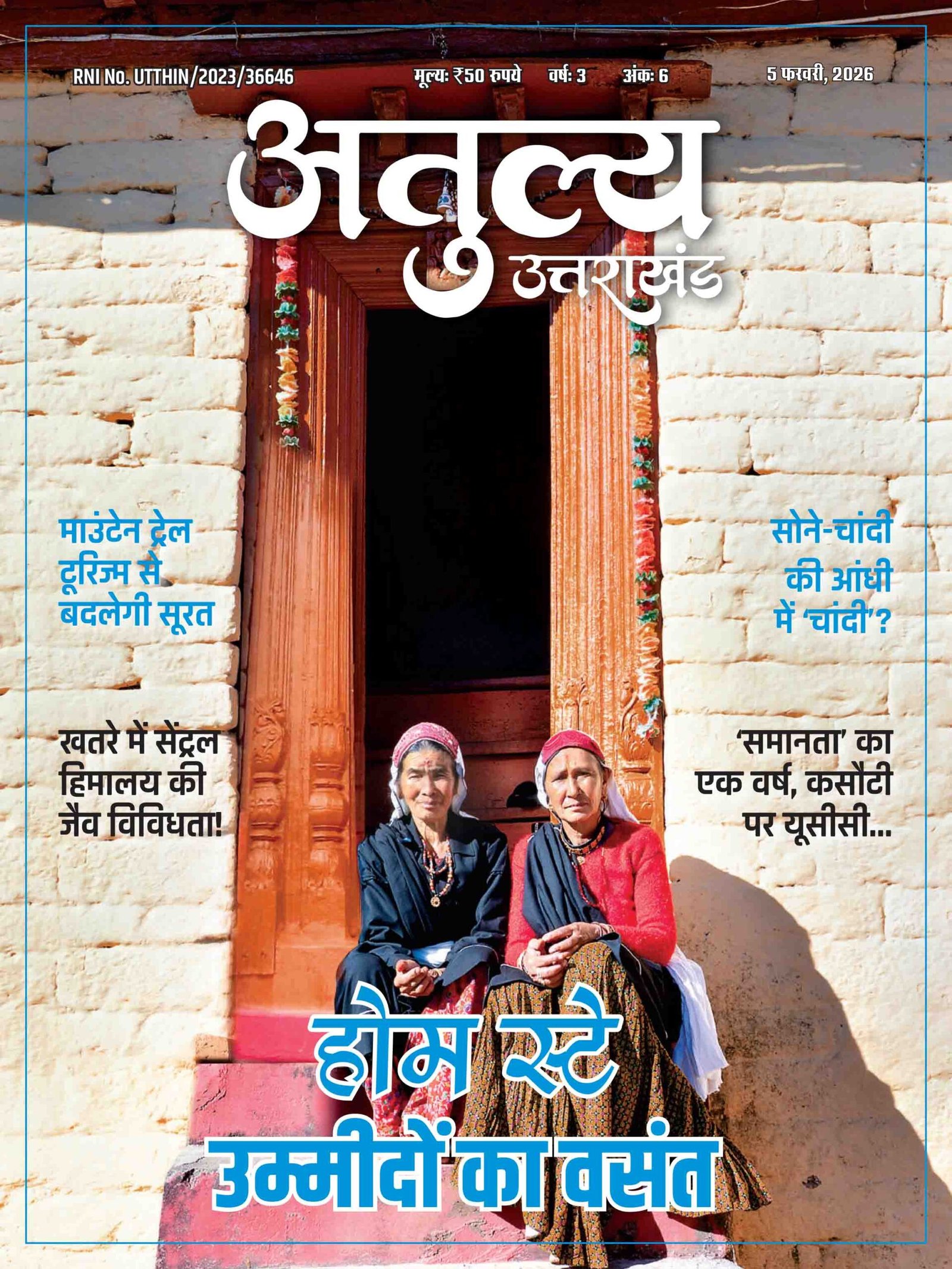सड़कें ऊंची होती जा रही हैं, मकान नीचे। यह बात हम अक्सर सुनते रहते हैं। यह हकीकत भी है। किसी भी शहर में आप जाइए वहां पर यह दृश्य आपको दिखाई दे जाएगा। निर्माणदायी संस्था साल दर साल सड़क के ऊपर सड़क बनाती चली जाती हैं। परिणामस्वरूप सड़क के लेवल से नीचे हुए घरों में बारिश के दौरान जलभराव होना आम समस्या हो गई है। लेकिन, अब इससे निजात मिल जाएगी। उत्तराखंड में भी एफडीआर (FDR Technology) तकनीक से सड़कें बनाई जाएंगी। अभी यह प्रयोग उत्तरकाशी की 42 किलोमीटर लंबी सड़क पर होगा। अगर यहां यह तकनीक सफल रहती है तो राज्य के अन्य हिस्सों में इस तकनीक का इस्तेमाल कर सड़कें बनाई जाएंगी।
राज्य में कई मार्गों पर ट्रैफिक दबाव पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा है। इसकी वजह से सड़कें जल्द ही क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसलिए इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे तो चार से पांच राज्य इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी एफडीआर तकनीकी से सड़कें बन रहीं हैं। अगर यहां पर यह सफल रहता है तो अन्य सड़कें भी इसी तकनीक से बनाईं जाएंगी। क्योंकि इसकी लागत पारंपरागत सड़कों से 20 से 25 फीसदी सस्ती लगती है। मीडिया से बातचीत में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख दीपक यादव बताते हैं, शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। वह कहते हैं इससे सड़कों के ऊंची होने की शिकायत भी कम हो जाएगी।
एफडीआर यानी फुल डेप्थ रिक्लेमेशन एक रिसाइकलिंग तकनीक है। इसके जरिये कम संसाधनों में मजबूत, टिकाऊ सड़कें बनाई जाती हैं। इसमें, खराब हो चुकी सड़क को उखाड़कर उससे मिलने वाले मटेरियल में केमिकल मिलाकर नया मटेरियल तैयार किया जाता है। फिर उसे नई सड़क बनाने में उपयोग किया जाता है। इससे ऊंची होती सड़क से निजात तो मिलेगी साथ ही बचत भी होगी। FDR तकनीक में डामर फुटपाथ को रोडवे रिक्लेमर मशीन से पीसा जाता है।
FDR तकनीक से बनी सड़कें मजबूत होती हैं और इन्हें कम रखरखाव की जरूरत होती हैं। इस तकनीक में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। साथ ही यातायात के बीच काम किया जा सकता है, इसलिए यह स्थानीय निवासियों के लिए सुविधाजनक होती है।
कैसे बनती है सड़कें
इस तकनीक के तहत गिट्टी युक्त पुरानी सड़क को आधुनिक मशीनों से उखाड़कर उसे बारीक टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाता है। उधेड़ी गई सड़क की पपड़ी को रिसाइकिल कर सड़क पर बिछाकर समतल किया जाता है। सीमेंट में चिपकने वाले केमिकल के तौर पर एडिटिब्स को मिलाकर उसका घोल तैयार कर समतल किए गए हिस्से पर सतह के रूप में डाला जाता है। फिर इसे रीसाइक्लर और मोटरग्रेडर उपकरणों से रोल करने के बाद पैडफुट रोलर और काम्पैक्टर से दबाया जाता है। इसके बाद सात दिनों तक पानी से तराई की जाती है। फिर यातायात का दबाव झेलने के लिए सतह के रूप में स्ट्रेस अब्सॉर्बिंग इंटरलेयर तैयार की जाती है। इसके बाद हवा के प्रेशर से अच्छी से सड़क की धूल को साफ करने के बाद उस पर फैब्रिक कपड़े को बिछाया जाता है, ताकि वह नमी को सोख ले। डामर का छिड़काव करने के बाद फिर मटेरियल डालकर रोलर घुमाया जाता है। इसके ऊपर पेवर मशीन से बिटुमिन कंक्रीट बिछाकर उस पर रोलर चलाया जाता है।

परंपरागत सड़कों की तुलना में 20 से 25 फीसदी सस्ता
परंपरागत तरीके से निर्मित सड़क की तुलना में यहां पर 20 से 25 प्रतिशत तक लागत में कमी आती है। साथ ही सड़क निर्माण के क्षेत्र में पत्थर, मिट्टी, बोल्डर आदि न होने के बावजूद भी सड़क का निर्माण अच्छा और मजबूत किया जाता है, क्योंकि पुरानी सड़क में लगे मैटेरियल को हो रिसाइकिल किया जाता है। पुराने मैटेरियल को उखाड़ कर सड़क बनाने से सड़क को ऊंचाई नहीं बढ़ती। जिससे रहवासियों को सड़क और आउटर के लेवल में फर्क देखने को नहीं मिलता। इसमें पुरानी रोड की गिट्टी समेत अन्य चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। सड़क को जापान और नीदरलैंड की मशीन से सीमेंट और केमिकल के तौर पर एडिटिब्स को मिक्स करके बनाया जाता है। इसके बाद एक लेयर केमिकल की बिछाई जाती है। विदेशों में इसी तकनीक से रोड को बनाया जाता है।

इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य है यूपी
करीब तीन वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में चित्रकूट से FDR तकनीक पर सड़क निर्माण की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली अधिकांश सड़कें इसी तकनीक से बनाई जा रही हैं।